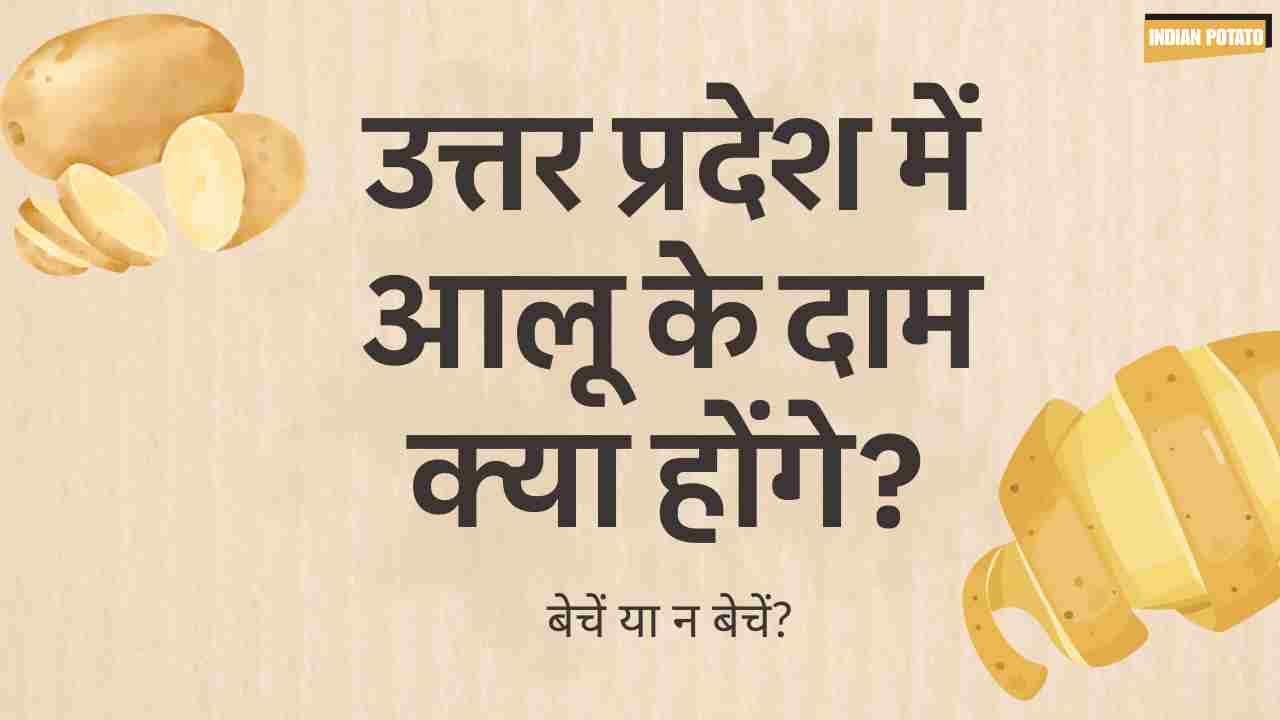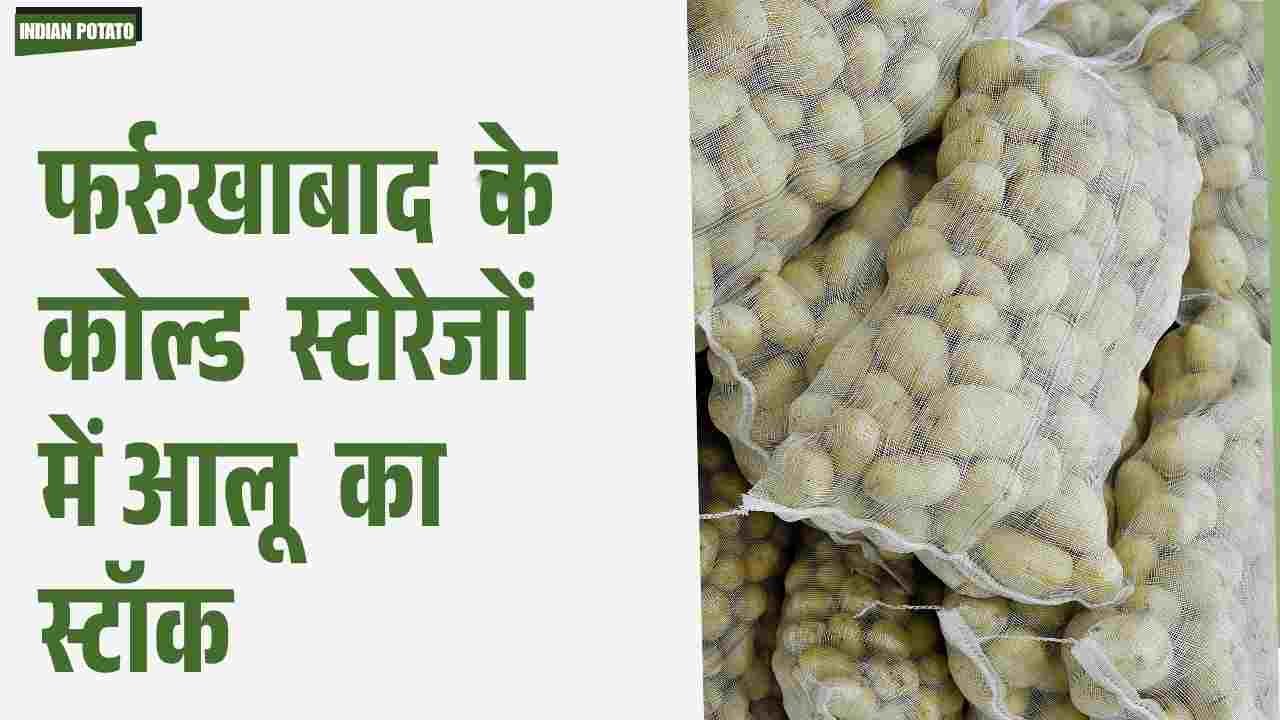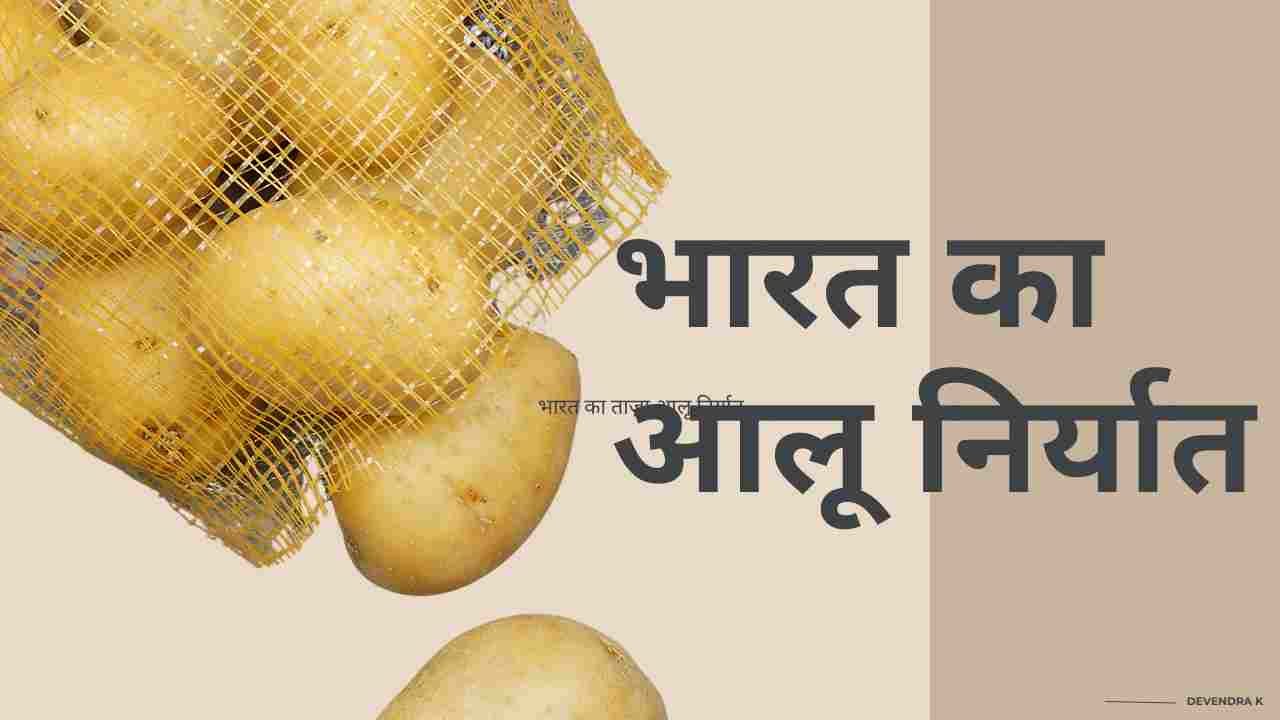ओडिशा के किसान हाल ही में आलू उगाने के नए तरीके सीखने के लिए शिमला की एक महत्वपूर्ण यात्रा पर गए थे। उनका लक्ष्य केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) में उन्नत तकनीकें सीखना था ताकि अपनी आय दोगुनी कर सकें और अपने गृह राज्य में खेती को और अधिक सफल बना सकें।
यद्यपि ओडिशा में अच्छी ज़मीन है, फिर भी वहाँ के आलू किसानों को संघर्ष करना पड़ा है। उन्हें पुरानी खेती के तरीकों से कम पैदावार, ढेर सारे कीटों और बीमारियों, और आधुनिक खेती के बारे में पर्याप्त जानकारी न होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आलू की कीमतें घटती-बढ़ती रहती हैं, अच्छे बीज मिलना मुश्किल होता है, और कटाई के बाद उनकी बहुत सी फसल बर्बाद हो जाती है। इससे उनके लिए अच्छा मुनाफ़ा कमाना मुश्किल हो जाता है। उन्हें अलग-अलग मौसम में काम करने वाली खेती के तरीकों के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो बदलते मौसम वाले इलाके में एक बड़ी समस्या है।
इन जारी समस्याओं से निपटने में मदद के लिए, शिमला स्थित एक प्रमुख आलू अनुसंधान केंद्र, सीपीआरआई ने 9 से 11 जुलाई तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह टीम वर्क दर्शाता है कि विभिन्न स्थानों पर ज्ञान और कौशल का आदान-प्रदान खेती को स्थायी रूप से विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। बरहामपुर और गंजम सहित ओडिशा के विभिन्न हिस्सों से 27 किसान इसमें शामिल हुए और उन्होंने दिखाया कि वे सीखने और अपनी पुरानी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हैं।
सीपीआरआई में प्रशिक्षण की योजना आधुनिक आलू की खेती के बारे में सब कुछ सिखाने के लिए सावधानीपूर्वक बनाई गई थी। किसानों को आलू की नई किस्मों के बारे में सिखाया गया जो अधिक उत्पादन देती हैं और रोगों का बेहतर प्रतिरोध करती हैं, जिससे उनकी उपज में वास्तव में वृद्धि होनी चाहिए। कार्यक्रम का एक प्रमुख भाग हानिकारक रसायनों को कम करने वाले तरीकों का उपयोग करके प्राकृतिक रूप से कीटों का प्रबंधन करने पर केंद्रित था। इसका मतलब है स्वस्थ आलू और स्वस्थ वातावरण।
प्रशिक्षण का मुख्य फोकस सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों पर था, जो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में बहुत मददगार हैं। इन कुशल सिंचाई विधियों को सीखकर और उनका उपयोग करके, किसान कम पानी का उपयोग कर सकते हैं, कम बर्बादी कर सकते हैं, और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी फसलों को पर्याप्त नमी मिले। इससे खराब मौसम में भी बेहतर फसल प्राप्त होती है। उन्होंने यह भी सीखा कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीज कैसे उगाएँ, स्वस्थ पौधों के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें, और अपनी फसल को अच्छी तरह से कैसे संग्रहीत करें। फसलों का उचित भंडारण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे किसानों को फसल के बाद नुकसान से बचने में मदद मिलती है और वे अच्छे दामों पर अपने आलू बेच पाते हैं।
सीपीआरआई के निदेशक डॉ. ब्रजेश सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत की और बताया कि यह प्रशिक्षण कितना उपयोगी हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ओडिशा में इन नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए, तो आलू की पैदावार दोगुनी हो सकती है और किसान ज़्यादा कमा सकते हैं। संस्थान में सामाजिक विज्ञान के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. आलोक कुमार ने भी इस बात पर सहमति जताई और ओडिशा के किसानों के लिए बेहतर पैदावार और आय की संभावनाओं पर प्रकाश डाला।
टीमवर्क सिर्फ़ कक्षा में सीखने तक सीमित नहीं था। प्रशिक्षण में व्यावहारिक प्रदर्शन और चर्चाएँ भी शामिल थीं, जिससे किसान सीपीआरआई के विशेषज्ञों से सीधे बात कर सके। इस व्यावहारिक दृष्टिकोण ने यह सुनिश्चित किया कि उन्होंने जो सीखा वह सिर्फ़ सैद्धांतिक न होकर उनके अपने खेतों में सीधे इस्तेमाल किया जा सके। सीपीआरआई के कई अनुभवी वैज्ञानिक और इंजीनियर, जैसे डॉ. संजीव शर्मा, डॉ. विनोद कुमार और इंजीनियर सुब्रविंद जायसवाल, किसानों के साथ अपना गहन ज्ञान साझा करने के लिए वहाँ मौजूद थे।
सीपीआरआई का यह प्रयास और ओडिशा के किसानों की सक्रिय भागीदारी राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए बहुत उम्मीद जगाती है। आधुनिक तरीकों को अपनाकर, टिकाऊ खेती करके और मिलकर काम करके, ओडिशा के आलू किसान अब अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हैं। शिमला की पहाड़ियों से ओडिशा के खेतों तक का यह सफ़र सिर्फ़ जानकारी साझा करने से कहीं बढ़कर है; यह साबित करता है कि मिलकर काम करने से भारतीय कृषि का भविष्य उज्जवल और ज़्यादा सफल हो सकता है।